महान सम्राट अशोक का इतिहास हिंदी में (Samrat Ashok history in hindi) बिन्दुसार की मृत्यु की उपरान्त अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा
नमस्कार दोस्तों आज हम इस लेख में (Samrat ashok history in hindi) सम्राट अशोक का इतिहास जानने वाले है यदि आप महान सम्राट अशोक मौर्य का इतिहास हिंदी में जानना चाहते है तो इस लेख में शुरु से लेकर अंत तक बने रहे।
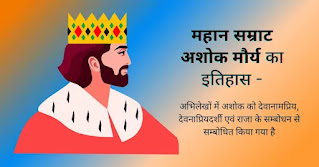 |
| Samrat Ashok History in Hindi |
सम्राट अशोक का इतिहास हिंदी में (Samrat Ashok history in hindi) बिन्दुसार की मृत्यु की उपरान्त अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। करीब चार वर्ष के सत्ता-संघर्ष के बाद अशोक का विधिवत् राज्याभिषेक करीब 269 ई0 पू0 में हुआ वैसे तो अशोक 273 ई0 पू0 में ही मगध के राजसिंहासन पर बैठ चुका था। अभिलेखों में अशोक को देवानामप्रिय, देवनाप्रियदर्शी एवं राजा के सम्बोधन से सम्बोधित किया गया है। सर्वप्रथम मस्की अभिलेख में अशोक नाम मिलता है। गूर्जरा लेख में भी इसका नाम अशोक ही मिलता है। अपने राज्याभिषेक के सातवें वर्ष में अशोक ने कश्मीर एवं खोतान क्षेत्र के अनेक भागों को विजित कर मौर्य साम्राज्य में मिलाया। अशोक के प्राप्त सभी अभिलेखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका साम्राज्य उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत (अफगानिस्तान), दक्षिण में कर्नाटक पश्चिम में काठियावाड़ एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक था। कल्हण की राजतरंगिनी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी को किनारे 'श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की तथा नेपाल में ललितपत्तन नगर बचाया।
एक युग पुरुष के रूप में अशोक ने मौर्य साम्राज्य को अपनी नीतियों माध्यम से नई दिशा दी। वह अत्यधिक व्यापक दृष्टि से युक्त व्यक्तित्व था। उसने तत्कालीन समस्याओं को समझते हुए उन्हें सुलझाने का प्रयास किया। उसका धम्म एवं अन्य नीतियाँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी तत्कालीन समय में थी। ये सार्वजनिक, सार्वभौगिक व सार्ययुगीन है, जो एक अकेले राष्ट्र की धरोहर नहीं हो सकती। सम्पूर्ण विश्व की धरोहर है, ऐसी नीतियों के प्रवर्तक के रूप में हम अशोक को महान् कहते है। अशोक ने पितृवत शासन का सिद्धान्त दिया तथा लोककल्याण को राज्य का सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य बनाया व कौटिल्य के लोक कल्याण के आदर्श को आत्मसात् किया। वृक्षारोपण, कृषि, सिंचाई सार्वजनिक निर्माण (कुए, सराय आदि) के कार्य कराये इनसे रोजगार का सुधार हुआ आर्थिक एवं आधारभूत संरचना में व्यापक सुधार हुआ एवं राज्य को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत बनाया, जो आज भी प्रासंगिक है।
अशोक ने धम्म का प्रतिपादन करके राजा, प्रजा एवं नौकरशाही हेतु संहिता तैयार की। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक एकता व विकास को बढ़ावा दिया. जिससे अन्तःसंबंधों में प्रगाढता आई। उसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण करना था। अशोक एक मात्र ऐतिहासिक शासक हुए, जिसने प्रजा से प्रत्यक्ष सम्पर्क किया। इस हेतु अशोक ने धम्म यात्राएँ की एवं प्रतिवेदका आदि अधिकारियों की नियुक्तियों की।
भौतिक संस्कृति के प्रचार-प्रसार एवं शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए उसने समाज को कमजोर वर्गों को गतिशीलता प्रदान की कृषि भूमि का विस्तार किया तथा युद्ध बन्दियों आदि को वनों व खानों में लगा दिया वे एक मात्र ऐसे शासक हुए जिन्होनें प्रजा के आध्यात्मिक व नैतिक उत्थान के साथ-साथ उत्पादन शक्तियों पर भी ध्यान दिया। अशोक ने ग्रामीण विकास को ध्येय बनाया तथा इस पर अधिक ध्यान दिया। अशोक ने साम्राज्य में 84000 स्तूपों का निर्माण कराया। राजस्व का पुनर्वितरण सार्वजनिक हित एवं लोकानुरंजन कार्य में किया तथा अर्थव्यवस्था को तीव्रता व गति दी। इन कार्यों के फलस्वरूप आम जनता की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई।
अशोक ने वैदेशिक नीति को समसामयिक बना दिया तथा तत्कालीक सम्राटों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए एवं उच्च स्तरीय धम्म आयोग भेजे, जिससे अन्तःसंबंधों की स्थापना हुई। अशोक ने सम्पूर्ण विश्व को धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया, सभी धर्मों को समान महत्त्व व आदर प्रदान करने पर बल दिया तथा जनता पर धर्म को बलात् नहीं थोपा एक धर्म, एक भाषा, प्रायः एक लिपि का अनुसरण कर सम्पूर्ण भारतवर्ष का एकीकरण किया। समान नागरिक संहिता व दण्ड संहिता का क्रियान्वयन कर सामाजिक न्याय एवं कानून के शासन की स्थापना की। विभिन्न वर्गों व धर्मों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए, जो प्रगतिशील अर्थव्यवस्था तथा राज्य की प्रगति हेतु नितान्त आवश्यक है।
अशोक ने अपने अभिषेक के आठवें वर्ष में लगभग 261 ई0 पू0 में कलिंग पर आक्रमण किया। हाथीगुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि सम्भवतः कलिंग पर नंदराज नाम का राजा शासन करता था। उस समय कलिंग की राजधानी तोशली थी। अशोक सम्पूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधना चाहता था एवं कलिंग हाथियों हेतु प्रसिद्ध होने एवं व्यापार-व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। समुद्र के किनारे होने के कारण विदेशी व्यापार की दृष्टि से इसका महत्त्व था। कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गये व 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। इस भीषण नरसंहार से अशोक का मन द्रवित हो गया तथा उसने भविष्य में युद्ध की नीति को त्यागने की घोषणा की. अब अशोक ने भेरी घोष को त्याग करें धम्म घोष को अपनाया।
अशोक के बाद, जालोक, कुणाल, दशरथ, सम्प्रति शालिशूक, देववर्मन आदि शासकों ने शासन किया। बृहद्रथ अन्तिम मौर्य सम्राट था। बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र ने 185 ई० पू० में उसकी हत्या कर एक नये शुंग साम्राज्य की नींव रख
"अशोक का धम्म"
अशोक धम्म के प्रमुख सिद्धांत
- सहिष्णुता : जन सामान्य के मध्य आत्म सहिष्णुता, विभिन्न विचारों, धर्मों एवं आस्थाओं के मध्य सहिष्णुता।
- अहिंसा : सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का सिद्धान्त प्रतिपादित किया।
- आडम्बरहीनता : धर्मानुष्ठानों तथा बलि चढ़ाने को अर्थहीन कहा।
- लोककल्याण : वृक्षारोपण, कुएँ एवं सरायों आदि का निमार्ण कार्य ।
- श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता श्रेष्ठ नैतिक, पवित्र आचरण, सदाचार एवं सत्यवादिता पर बल दिया।
विभिन्न वर्गो, जातियों और संस्कृतियों को एक सूत्र में बाँधने तथा अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की, उसे अभिलेखों में 'धम्म' कहा गया है। धम्म के सिद्धान्त हर धार्मिक सम्प्रदाय से संबंध रखने वाले लोगों के लिए स्वीकार्य थे। अशोक के अभिलेखों में उस व्यापक नीति अर्थात् धम्म का उल्लेख किया गया, जो सामान्य व्यवहार को नए ढांचे में ढालने के लिए आवश्यक थी।
'धम्म' के बुनियादी सिद्धान्तों में अशोक ने सर्वाधिक बल सहिष्णुता पर दिया। प्रथम स्वयं व्यक्तियों की सहिष्णुता, द्वितीय विभिन्न विचारों, विश्वासों, धर्मों एवं भाषाओं में सहिष्णुता इसे अशोक ने 7. 11 व 12वें शिलालेख व दूसरे लघु शिलालेख में उल्लेखित किया। जिसमें माता-पिता की सेवा, गुरुओं का आदर, दासों के साथ उचित व्यवहार, धर्म -सार की वृद्धि, वाकसंयम तथा समवाय पर बल दिया। धम्म का दूसरा बुनियादी सिद्धान्त अहिंसा था, जिसका तात्पर्य युद्ध व हिंसा द्वारा विजय प्राप्ति का त्याग और जीव हत्या का विरोध था जो प्रथम व 11वें शिलालेख व पांचवें स्तम्भ लेख में मिलते हैं।
सम्राट अशोक के जनकल्याणकारी कार्य - धम्म नीति में ऐसे कार्य भी शामिल थे, जो आम नागरिकों के कल्याण से संबंधित थे जो सातवें स्तम्भ लेख व दूसरे शिलालेख में लिखित है, जिसमें वृक्षारोपण, सराय, ससके, सिंचाई, कुओं के निर्माण आदि की व्यवस्था थी अशोक ने नवे शिलालेख में विश्वासों के फलस्वरूप जो निरर्थक अनुष्ठान और यज्ञ होते थे, ऐसे बाढ्याडम्बरों की निदा की। प्रथम स्तम्भ लेख में धम्म की प्राप्ति के लिए धर्म यात्रा, धर्म मंगल, धर्म दान, शुश्रूषा आदि की व्यवस्था की।
अशोक दूसरे स्तम्भ लेख में धम्म की परिभाषा बताते हुए कहता है "अपासिनवे बहुकथाने दया दाने सचे सोचये माधवे साधवे च" अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति पापों से दूर रहे. कल्याणकारी कार्य करे, दया, दान, सत्य, पवित्रता मृदुता का अवलम्बन करे। तीसरे स्तम्भ लेख में वह प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमण्ड एवं ईर्ष्या आदि के निषेध का कहता है, इनके लिए व्यक्ति आत्म निरीक्षण अर्थात् 'निज्झति' करे एवं सबके साथ श्रेष्ठ व्यवहार करे।
धम्म को फ्लीट ने राजधर्म, राधाकुमुद मुखर्जी ने सार्वभौम धर्म एवं भण्डारकार ने उपासक बौद्ध धर्म कहा। यद्यपि अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध था। महावंश व दीपवंश के अनुसार अशोक ने मोगलिपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में तृतीय बीद संगीति (सभा) बुलाई और मोगलिपुत्र तिस्स की सहायता से संघ में एकता और अनुशासन लाने का प्रयास किया। इससे उसके बौद्ध होने की पुष्टि होती है। तथापि धम्म में सर्वमान्य आचार तत्वो और नैतिक नियमों का समन्वय था तथा धम्म अत्यन्त ही सरल, सुबोध, पवित्र, नैतिक और व्यावहारिक था। उसका धम्म सर्वमंगलकारी था, जिसका उद्देश्य प्राणिमात्र का उद्धार करना था।
अशोक धम्मा की नीति की क्रियांवति - अशोक ने धम्म के प्रतिपादन हेतु व्यावहारिक उपाय किए। इस हेतु अशोक ने न केवल युद्ध की नीति का परित्याग किया, अपितु आम जन के दुःख दर्द एवं उनकी आवश्यकताओं को भली भाँति समझा। उसने नौकरशाहों को तत्काल न्याय देने तथा लोकहित के कार्य करने हेतु पाबन्द किया।
अशोक ने सार्वजनिक हित के कार्य किए यथ परिवहन, सिंचाई. कुओं, सरायों आदि का निर्माण कराया इन समस्त सार्वजनिक हित के कार्यों का उद्देश्य धम्म को स्वीकार कराना था। अशोक ने धम्म के उपदेशों को पाषाणों पर उत्कीर्ण कराया तथा ऐसी जगहों पर लगाया जहाँ पर आम जन पढ़ सके, इस तरह अशोक ने धम्म को सार्वजनिक एवं सार्वभौम बना दिया। हिंसा पर प्रतिबंध लगाया तथा पशुबलि को निषेध किया समान नागरिक आचार संहिता, दण्ड संहिता के सिद्धान्त को जन्म दिया तथा क्रियान्वित किया। जगह-जगह धम्म आयोग भेजे एवं विदेशों में भी धम्म का प्रचार-प्रसार किया। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की व उनके दायित्वों का प्रतिपादन किया।
अशोक धम्म की नीति का मूल्यांकन - यद्यपि धम्म के मूल सिद्धान्त सहिष्णुता, अहिंसा एवं सदाचार थे, जो कि भारतीय संस्कृति के प्रारम्भ से ही के मूल तत्त्व रहे हैं तथा वर्तमान में भी उनका महत्त्व यथावत है। अशोक के बाद के सभी शासकों ने इन सिद्धान्तों को स्वीकार किया. तथापि समग्र रूप से यह नीति अशोक के पश्चात् फलीभूत नहीं हो सकी, इसके अनेक कारण थे धम्म की नीतियों का अशोक के उत्तराधिकारी उसी रूप में क्रियान्वित नहीं कर सके । धम्म दुर्बल शासकों, राजनीतिक अनिश्चितता व सीमाओं की असुरक्षा के कारण फलीभूत नहीं हो सका, क्योंकि धम्म की नीति का कार्यान्वयन शान्तिकाल में ही संभव है, जब राष्ट्र आन्तरिक व बाहरी रूप से युद्धों से पूर्णतया मुक्त हो। परवर्ती शासक अशोक की दूरदर्शिता को नहीं समझ पाये, धम्म महामात्र अपने असीमित अधिकारों द्वारा जनता के कार्यों में अवांछनीय हस्तक्षेप करने लग गये। सामाजिक तनाव ज्यों के त्यों बने रहे एवं साम्प्रदायिक संघर्ष बराबर चलते रहे, क्योंकि समस्याएं व्यवस्था की जड़ों में निहित थी।
उपर्युक्त कारणों से धम्म की नीति फलीभूत नहीं हो सकी, तथापि अशोक सराहना का पात्र है कि उसने एक पथ प्रदर्शक सिद्धान्त की आवश्यकता को महसूस करते हुए धम्म की नीति का प्रतिपादन किया, जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है।
ये भी पढ़े:
- महाराणा प्रताप का इतिहास व जीवन परिचय - Maharana Pratap History & Biography in Hindi
- पृथ्वीराज चौहान का इतिहास और जीवन परिचय - Prithviraj Raj Chauhan History and biography in Hindi
- राव चंद्रसेन का इतिहास और जीवन परिचय - Rao Chandrasen History and Biography in Hindi
- वीर गोगाजी का इतिहास और जीवन परिचय - Veer Gogaji History & Biography in Hindi




.webp)




COMMENTS